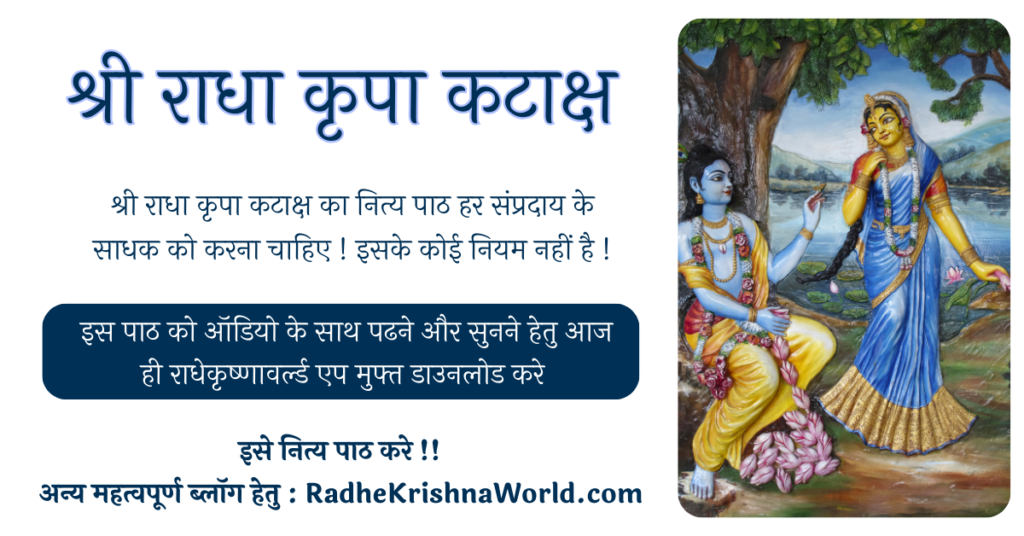विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में वर्तमान पंचकोसीय वृन्दावन हिंसक जीव-जन्तुओं से सेवित एक घने जंगल के रूप में स्थित था। इसे श्रीयमुनाजी ने चारों ओर से घेरा हुआ था तथा यह बहुत बड़े बद के रूप में प्रवाहित होती थी, जिसमें बड़ी घड़ी व्यापारिक नायें चला करती थीं, क्योंकि उस समय जल मार्ग से ही विशेषतः व्यापार हुआ करता था। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बस्ती तो थी ही नहीं, किन्तु इसके परिसर में तथा आस-पास के स्थानों में बटमार वृत्ति के लोगों ने अपने रहने एवं लूट के सामान को घने जंगलों में छिपाकर रखने के ठिकाने अवश्य बना रखे थे। ये मवासी लोग श्रीयमुनाजी से गुजरने वाले व्यापारियों के सामाव पर जकात (चुंगी अथवा कर) भी वसूल किया करते थे, जिससे इन्हें काफी आमदनी हो जाया करती थी।
इन लुटेरों में अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण, वृन्दावन से पश्चिम की ओर कई मील दूर शेरगढ़ के आगे यमुना तट पर स्थित भैगाँव निवासी नरवाहन नामक लुटेरा प्रमुख था। उसकी आज्ञाओं को न मानने का साहस किसी में भी नहीं था। उसने अपने पराक्रम से एक सशस्त्र सेवा बनाकर स्वयं को राजा के रूप में स्थापित कर लिया था तथा अपनी शक्ति के बल पर सम्पूर्ण व्रज पर अपना अधिकार बना लिया था। उसकी इस शक्ति से बड़े-बड़े राजा-महाराजे भी डरते थे। यहाँ तक कि दिल्लीश्वर का भी दस्युराज नरवाहन पर कोई नियंत्रण नहीं था।
उन्हीं दिनों विक्रम संवत् 1590 की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन गोस्वामी श्रीहित हरिवंश चन्द्र जी ने इस जन शून्य पंचकोसी वृन्दावन में प्रथम पदन्यास किया था। वे अकेले नहीं थे। उनके साथ देवयत से आये उनके कुछ शिष्यगण, मार्ग में चिरथावल में नव विवाहिता उनकी दोनों पनियाँ एवं दहेज के रूप में मिले उनके परमेष्ट श्रीराधावल्लभलालजी का सेव्य स्वरूप भी था। श्रीहिताचार्य के अभूतपूर्व रूप सौन्दर्य को देखकर पंचकोसी वृन्दावन के विकटवर्ती ब्रजवासीगण इकट्ठे हो गये। श्रीहिताचार्य ने उन ब्रजवासियों से स्वयं सपरिवार वृन्दावन में निवास करने की अभिलाषा प्रकट की। यह जानकर उन ब्रजवासियों को अत्यधिक आश्चर्य और हार्दिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय श्रीहिताचार्य के हाथ में तीर कमान देते हुए कहा- “गुसाँईजी ! आप यह तीर चलाइये, आपका यह तीर जहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक की भूमि आपके अधिकार में होगी।” श्रीहिताचार्य ने यमुना तट पर स्थित जिस ‘ऊँची टेर’ से तीर फेंका था, उसी स्थल पर अपना निवास स्थान बनाया और वहीं पर लताओं से बनाये गये मन्दिर में श्रीराधावल्लभलालजी को विराजमान करके वे उनकी अष्टयामी सेवा करने लगे।
अपने गुप्तचरों के द्वारा दस्युराज बरवाहन को जब यह ज्ञात हुआ कि कोई ऐसा चमत्कारी महापुरुष हिंसक जन्तुओं से संसेवित निर्जन वन में आया है, जिसके मधुर प्रभाव से हिंसक जन्तु तथा निर्जन यन के परिसर में बसे बटमारों के मन-बुद्धि और चित्त बदल गये हैं तथा वे सब उस महापुरुष की सेवा-सुश्रूषा में लग गये हैं; तो कुतूहल देखने की दृष्टि से एक दिन वह भी श्रीहिताचार्य के निवास स्थान पर आया। उस समय श्रीहिताचार्य अपने शिष्यों एवं ब्रजवासियों से घिरे हुए थे और ‘नवल’ नामक शिष्य के साथ कुछ आलाप- संलाप कर रहे थे। राजा नरवाहन भी श्रीहिताचार्य के मधुर प्रभाव से अछूता न रह सका। वार्तालाप सुनकर उसे अपनी वृत्ति पर बहुत खेद हुआ। उसने अपना हार्दिक दुःख प्रकट करते हुए श्रीहिताचार्य से स्वयं को शरण में लेने की प्रार्थना की। श्रीहिताचार्य ने उसकी निष्कपट वाणी सुनकर उसे मन्त्रदान के साथ-साथ मधुर उपदेश भी दिये, जिससे उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। नरवाहन जैसे खूंखार दस्यु के जीवन में इस परिवर्तन से पंचकोसी वृन्दावन में निवास करना सबके लिये सुगम हो गया। उन्होंने स्वयं भी श्रीराधावल्लभलालजी के लिये मन्दिर बनाने का संकल्प लेकर उसे अतिशीघ्र पूरा किया। श्री नरवाहन जी द्वारा बनवाये गये इस नये मन्दिर में श्रीराधावल्लभलालजी को विक्रम संवत् 1591 की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन विराजमान कर, उनका प्रथम पाटोत्सव अत्यन्त धूमधाम एवं विशेष समारोह के साथ मनाया गया।
श्री नरवाहन जी ने श्रेष्ठ गुरु के उपदेश से अपने मन के सारे प्रश्नों का समाधान पा लिया था। अब वे अपना अधिकाधिक समय सेवा उपासना में देने लगे। अच्छे भावों के उदय होने से उन्हें स्वयं ही लगा कि चित्त निर्मल होता जा रहा है। धीरे-धीरे वे राजकार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गये और उनके कर्मचारी राज्य संचालन में उनकी जगह काम करने लगे।
एक दिन की बात है कि एक जैन व्यापारी व्यावसायिक सामानों से लदी हुई बड़ी-बड़ी नायों में यमुना में से जा रहा था। नियमानुसार राजकर्मचारियों ने उससे राज्य कर देने को कहा, किन्तु यह मदान्ध व्यापारी जिसके साथ सात सौ बन्दुकधारी एवं हजारों सैनिक थे, लड़ने के लिये तैयार हो गया। नरवाहन जी की फौज ने उसे पराजित कर दिया और उसे बन्दी बनाकर इनके सामने उपस्थित किया गया। विचार विमर्श के बाद आपने आदेश दिया कि इसका सारा धन जोकि तीन लाख था, राज्य कोष में जमा किया जाय तथा इतना ही धन और मैगावे पर इसे छोड़ा जाय और तब तक इसे गले में तींक तथा पावों में बेड़ी पहनाकर कैदखाने में डाल दिया जाय।
बहुत दिनों के बीत जाने पर भी व्यापारी धन नहीं मंगा सका और उसे मृत्युदण्ड की सजा सुना दी गई। इस फैसले को सजा की एक सेविका ने सुन लिया। दया और करुणा से भरी सेविका की आत्मा उस विरपराध व्यापारी के प्राण बचाने के लिये आकुल हो उठी। रोज के समय पर भोजन देने पहुंची उसने व्यापारी से कहा कि राजा की सभा में कल तुम्हें प्राणदण्ड देना तय हो गया है और बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी ने सेविका के चरण पकड़ लिये। घबराते हुये उसने प्रार्थना की कि मुझे अब बचने का कोई उपाय बताओ। सेविका ने उसे प्राण बचाने का आश्वासन देते हुए शान्त किया और कहा कि तुम मेरी ही तरह इस कंठी-माला और तिलक को धारण करो और हमारे राजा को श्रीराधावल्लभ और श्रीहरिवंश वाम से बड़ी प्रीति है, वे सदा उनका भजन करते रहते हैं, अतः तुम रात को “श्रीराधावल्लभ श्रीहरिवंश” की नाम-ध्वनि बहुत जोर-जोर से करना। इसी नाम के प्रभाव से तुम्हारे प्राप्ण बच जायेंगे। राजा के पूछने पर यह और कहना कि मैं श्री हरिवंश महाप्रभुपाद का शिष्य हैं। यह कहकर सेविका चली गई। इधर व्यापारी उसी क्षण से “श्रीराधावल्लभ श्रीहरिवंश” वाम ध्यति का जाप मन ही मन में करने लगा तथा अर्द्धरात्रि होने पर बड़े उच्च स्वर से उसे बोलता प्रारम्भ कर दिया। ऐसी सुनसान रात्रि में अपने गुरु-इष्ट का नाम सुनकर नरवाहन जी की नींद टूट गयी और यह कैदखाने की ओर दौड़ पड़े। वे व्यापारी के चरणों में गिर गये और व्यापारी से यह जानकर कि वह हित महाप्रभु का कृपापात्र है अत्यंत लज्जित एवं दुःखी होकर व्यापारी से क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि हमने आपको जैनी समझकर लूट लिया था, अब आप ये बात श्री गुरुदेव जी से मत कहना।
प्रातः काल होते ही व्यापारी को खान कराया गया, स्वच्छ कपड़े पहनाकर उसका सम्मानत किया गया, उसकी सारी सम्पत्ति लौटा दी गयी और उसका चरण स्पर्श करते हुए उसे आदर पूर्वक विदा किया गया। व्यापारी के हृदय पर इस घटना का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। व्यापारी ने सोचा कि जिनका झूठा नाम लेने पर मेरे प्राण बच गये, उनका निश्छल हृदय से नाम लेते एवं उनकी शरण लेने पर व जाने क्या प्राप्त होगा। यह सोचकर उसने वृन्दावन आकर श्रीहित महाप्रभु के दर्शन किये और अपना सारा धन श्रीहितप्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए अपना सब वृत्तान्त भी कह सुनाया। श्रीहिताचार्य वे भी उसकी हार्दिक श्रद्धा से द्रवीभूत होकर उसे मंत्र-दीक्षा प्रदान करते हुए हित-धर्म की रीति से परिचित कराया; साथ ही उसके द्वारा समर्पित की गई उसकी विपुल सम्पत्ति का स्पर्श न कर, यह कहते हुए, उसे ही लौटा दिया कि यह इस सारी सम्पत्ति को साधु-वैष्णवों की सेवा में लगाकर परम सुख का अनुभव प्राप्त करे। व्यापारी भी इस गुरु-आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने घर के लिये विदा हो गया।
व्यापारी के चले जाने के बाद श्री नरवाहन जी डरते हुए श्री हित जी महाराज के समीप आये और उनके कृपापात्र को अज्ञानवश इतनी अधिक पीड़ा देने के अपराध की क्षमा माँगी। महाप्रभुजी ने नरवाहन जी की अद्भुत गुरु-निष्ठा पर रीझकर उन्हें अपने गले से लगा लिया और उसी समय उन्हें अपने साथ ले जाकर परिकर सहित प्रिया-प्रीतम के दर्शन कराये तथा दो अत्यंत सुन्दर पदों की रचना उनके नाम से कर दी। भेंट में दिये वे दो पद श्रीहित चतुरासी की पद संख्या 11 तथा 12 हैं।
(धार्मिक जगत में शिष्यों द्वारा अपनी रचनाओं को, अपने गुरुओं के नाम से ही प्रचलित करने के अनेकानेक उदाहरण देखने में आते हैं; किन्तु गुरु द्वारा अपनी रचना अपने शिष्य को भेंट करने का उपर्युक्त उदाहरण अद्वितीय है और श्रीहिताचार्य की सहज प्रेमस्वरूपता का परिचायक है।)
( Source : Shri Rasik Ananymal Book )
Click Here to Order This Book From Vrindavan : RKWGallery.com